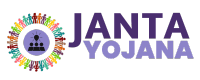Read in english: गोंड आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रामलाल नरते (68) मंडला ज़िले के कुंडा गांव में रहते हैं। यह गांव नर्मदा नदी से केवल 4 किमी दूर है। फिर भी नरते केवल बारिश की फसल ही ले पाते हैं। हम जब उनसे पूछते हैं कि वह गर्मी के दिनों में फसल क्यों नहीं ले पाते? वह कहते हैं,
“फसल तो खूब हो जाए साब, लेकिन पानी की सुविधा ही नहीं है।”
यह कहानी अकेले नरते की नहीं है। नर्मदा के एक ओर मंडला और दूसरी ओर सिवनी ज़िला है। मगर दोनों ही ओर के खेत नदी के पास होते हुए भी पानी के मोहताज हैं। कुंडा गांव यहां प्रस्तावित चुटका परमाणु विद्युत परियोजना से भी प्रभावित होने वाला है। यहां रह रहे अधिकतर लोग बरगी बांध परियोजना से पहले से ही विस्थापित हैं। अब चुटका परियोजना से इनमें से कई लोग फिर से विस्थापित हो जाएंगे।
ऐसे में इनका कहना है कि एक तो उन्हें जिस जलाशय के लिए विस्थापित किया गया था आज तक उसका पानी नहीं मिला। दूसरा सरकारी तंत्र उन्हें तो पानी नहीं पहुंचा सका मगर ऐसी परियोजना के लिए उन्हें फिर से विस्थापित कर रहा है जिसमें बड़ी मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ेगी।
/ground-report/media/media_files/2025/01/29/A63swfTHj41JqPoRukty.png)
बांध के लिए विस्थापित हुए मगर खेत सूखे
नरते अपने परिवार का पोषण करने के लिए 20 एकड़ में खेती करते हैं। इस खेत में सिंचाई और पीने के पानी के लिए वो अपने खेत में बने कुएं पर निर्भर हैं। मगर वह बताते हैं कि गर्मी में यह पानी फसल और परिवार की ज़रूरत के आगे कम पड़ जाता है। जब कुआं सूख जाता है तो उनके परिवार की महिलाओं को तकरीबन 2 किमी दूर लगे एक हैण्डपंप से पानी लाना पड़ता है।
लगभग 45 साल पहले नरते किसी और गांव में रहते थे। मगर वह गांव बरगी बांध परियोजना में डूब का शिकार हो गया। नरते उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी युवावस्था में ही आन्दोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। वह अपने और आस-पास के गांववालों के साथ मिलकर बांध से उनका गांव डुबो देने का विरोध कर रहे थे। वह 45 साल पहले के अपने संघर्ष को याद करते हुए कहते हैं,
“तब अधिकारी आते थे और कहते थे कि बांध से लोगों को पानी मिलेगा और सिंचाई बढ़ेगी तो फसल भी होगी. मगर आज न हमारे पास अपने पुरखों का घर है और ना ही खेत में पर्याप्त पानी है.”
जबलपुर से 34 किमी और प्रदेश की राजधानी भोपाल से 339 किमी दूर स्थित बरगी बांध का निर्माण 1974 में शुरू हुआ था। यह बांध नर्मदा नदी पर बने शुरूआती बांधों में शामिल है। 69 मीटर ऊंचे इस बांध के चलते जबलपुर, मंडला और सिवनी जिले का लगभग 26,797 हेक्टेयर हिस्सा डूब गया था।
68 साल के नरते को इस परियोजना से डूबे गांवों की संख्या अब भी याद है। वह बताते हैं, “162 गांव डूबे थे।”
इस परियोजना के चलते सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,14,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इसी पूरी कवायत के पीछे यह तर्क काम कर रहा था कि इससे 4.37 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसके अलावा डैम से 105 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था।
मगर अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह बांध केवल 24,000 हेक्टेयर भूमि ही सिंचित कर रहा है।
नरते अपनी परेशानी बताते हुए कहते हैं कि उनके गांव में केवल 1 फेज़ का कनेक्शन है जबकि उनकी मोटर चलाने के लिए उन्हें 3 फेज़ के कनेक्शन की ज़रूरत होती है। ऐसे में गर्मी के दिनों में जब उनके कुएं का जलस्तर नीचे चला जाता है तो उन्हें बाल्टी से पानी खींचकर निकालना पड़ता है।
/ground-report/media/media_files/2025/01/30/Ls9GRqwI7b7gOWOi21i5.png)
डूब का शिकार हुआ जीवन
नरते के अलावा कुंडा के कई लोगों से हमने जब यह पूछा कि बांध बनने के इतने साल बाद उनका जीवन कैसे बेहतर हुआ? गांव के लोग इसका जवाब गुस्से में देते हैं। यह गांव मंडला की नारायणपुर तहसील के अंतर्गत आता है। गांव का कितना विकास हुआ है? यह पूछने पर एक बुजुर्ग कहते हैं,
“आप खुदई नारायणपुर तक चले जाओ सड़क से, बुखार आ जेहे।”
वह बुजुर्ग इस क्षेत्र की सड़क की खस्ताहालत की ओर इशारा कर रहे थे। यहां के लोग बताते हैं कि बरगी बांध के निर्माण के दौरान उनसे बेहतर जीवन की बात कही गई थी मगर 45 साल गुज़र जाने के बाद भी यहां का विकास रुका हुआ ही है। नरते कहते हैं,
“ऊपर के गांव में तो और हालत ख़राब है, वहां कोई अपनी लड़की भी नहीं देना चाहता क्योंकि लड़कों के पास कोई काम ही नहीं है।”
कुंडा की तरह ही इस क्षेत्र के अन्य गांव भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नर्मदा नदी के ठीक किनारे पर स्थित टाटिघाट नामक गांव में दो महिलाएं हैण्डपंप से पानी भर रही हैं। उनके पास बहुत सारे बर्तन हैं। यह महिलाएं बताती हैं कि उन्हें दिन में 4 बार इतना ही पानी भरकर अपने घर ले जाना पड़ता है। वह कहती हैं कि नदी के किनारे रहते हुए भी उनके घर में नल का कनेक्शन नहीं है।
टाटिघाट के श्यामलाल बर्मन पेशे से मछुआरे हैं। मगर उनके पिता काश्तकार (किसान) हुआ करते थे। पहले उनका परिवार मैदान में रहता था उसका नाम भी टाटिघाट ही था। मगर गांव डूब जाने के बाद पठार पर इसी नाम से वर्तमान गांव बसाया गया। वह बताते हैं कि विस्थापित करते हुए अधिकारियों ने उनसे एक फसल का वादा किया था मगर अब उनका पुराना खेत 12 महीना पानी में डूबा रहता है।
इसके चलते बर्मन अब भूमि हीन हो गए हैं। बर्मन बताते हैं,
“हमारी 1.5 एकड़ ज़मीन बरसात के बाद डूब से बाहर आती थी जिसमें हम एक फसल और कुछ सब्ज़ी उगा लेते थे। अब वो भी 12 महीना डूबी रहती है।”
बर्मन अपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ अभी जिस घर में रहते हैं वह भी छोड़ना पड़ सकता है। उनका गांव चुटका परमाणु परियोजना से प्रभावित होने वाला है। इस बारे में जब वह फिर से विस्थापित होने का दुःख बता रहे थे तभी उनके एक अन्य साथी कहते हैं,
“सरकार इतने साल में हमारे घर तो पानी पहुंचा नहीं पाई मगर अब उसके पास प्लांट को देने के लिए पानी है।”
दरअसल साल 2009 में सरकार ने चुटका परमाणु विद्युत परियोजना को मंजूरी दी थी। यह परियोजना मंडला ज़िले के ही चुटका गांव में स्थापित की जानी है। कुल 1400 (2×700) मेगावाट की क्षमता वाली इस परियोजना में मुख्य तौर पर परमाणु रिएक्टर को ठण्डा रखने के लिए हर घंटे 9000 क्यूबिक मीटर पानी की ज़रूरत होगी। यह पानी बरगी बांध से ही लिया जाना है।
/ground-report/media/media_files/2025/01/30/Dw6n5S3E1uIrJY81ri0j.png)
लिफ्ट इरिगेशन के पानी का इंतज़ार करते लोग
नर्मदा नदी को पार कर हम मंडला से सिवनी जिले में दाखिल होते हैं। यहां के केदारपुर गांव में हमारी मुलाक़ात नारायण पटेल (58) से हुई। पटेल फिलहाल केदारपुर में ही रहते हैं मगर बरगी बांध से हुए विस्थापन से पहले वह बिजौरा नामक गांव में रहते थे। यहां उनके पास 10 एकड़ ज़मीन थी जो पूरी तरह डूब का शिकार हो गई।
फिलहाल पटेल 5 एकड़ में खेती करते हैं। उन्होंने रबी के सीजन में 2 एकड़ में गेहूं और 3 एकड़ में मटर की बुवाई कर रखी है। मगर सिंचाई के साधन सीमित हैं इसलिए उन्हें अपनी उपज से बहुत आशा नहीं है।
“हमने 40 फीट कुआं खुदवाया है मगर उससे भी दिन में 1 घंटा पानी ही मिल पाता है।”
पटेल के लिए खेती के भरोसे अपने परिवार का पोषण करना मुश्किल है। इसलिए वह 130 किमी दूर स्थित नरसिंहपुर जिले में गन्ने के खेतों में मज़दूरी करने जाते हैं। बरगी बांध से विस्थापित होने पर उन्हें अपनी 10 एकड़ ज़मीन के लिए कुल 11000 रु ही मुआवज़े के रूप में मिले थे। वह अपनी वर्तमान आर्थिक दशा के लिए बरगी बांध को ही ज़िम्मेदार मानते हैं।
गौरतलब है कि 1987 में जबलपुर के तत्कालीन कमिश्नर केसी दुबे ने अपनी रिपोर्ट ‘प्लांन फॉर रूफ़’ में बताया था कि बरगी बांध के वजह से कुल 26,797 हेक्टेयर ज़मीन डूबी थी। इसमें 14,750 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल थी। साथ ही इस परियोजना से 7000 परिवार विस्थापित हुए थे। इनमें 43% आदिवासी समुदाय के लोग थे।
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि नरते की तरह ही पटेल का गांव भी नर्मदा से केवल 4 किमी ही दूर है। वह बताते हैं कि लगभग 10 साल पहले प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहां लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई परियोजना की घोषणा की थी। मगर यह घोषणा आज तक अमल में नहीं लाई गई है।
मंथन अध्ययन केंद्र में जलाशयों विशेषकर बांध आधारित सिंचाई परियोजनाओं पर शोध करने वाले रेहमत किसानों तक पानी न पहुंचाने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं,
“सरकार माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के मॉडल पर गंभीर नहीं है। वह इन योजनाओं में निवेश तो कर कर रही है मगर इसका कोई हिसाब नहीं है कि यह पैसा जा कहां रहा है।”
वह कहते हैं कि सरकार ने सिंचाई का कोई भी इन्फ्रास्ट्रक्चर ही विकसित नहीं किया है जिसके कारण 10 सालों में एक भी लिफ्ट इरिगेशन योजना सफल नहीं हो पाई है।
सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बरगी डाईवर्जन मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की लागत 1101.23 करोड़ रूपए थी। इस लागत से प्रदेश के जबलपुर, सतना, कटनी, रीवा और पन्ना ज़िले को पानी पहुंचाया जाना था। हालांकि बाद में इसकी लागत 5127.22 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।
मगर अब भी इस प्रोजेक्ट में मंडला और सिवनी के गांव शामिल नहीं हैं। यानि जो किसान बरगी बांध परियोजना से विस्थापित होकर अभी नर्मदा के किनारे रह रहे हैं उनको ही इसका पानी नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में सिवनी जिले के किंदरई में एक नए परमाणु विद्युत् परियोजना को मंज़ूरी दी है। यह परियोजना भी नर्मदा के किनारे और चुटका परमाणु विद्युत परियोजना के एकदम पास में स्थापित की जाएगी। ज़ाहिर है इसके लिए भी बड़ी मात्रा में बांध से पानी लिया जाएगा।
ऐसे में नरते और उनके जैसे विस्थापित हुए अन्य किसानों का कहना है कि सरकार को पहले उन्हें पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उनका कहना है कि सरकार पहले से ही सिवनी जिले में स्थित झाबुआ पॉवर प्लांट को पानी दे रही है। इसके बाद चुटका और फिर किंदरई को पानी दिया जाएगा। यानि विस्थापित हुए लोगों तक पानी पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में भी नहीं है।
कृषि और जलाशयों के मामले में विशेषज्ञता रखने वाले डॉ प्रदीप नंदी कहते हैं कि मध्य प्रदेश के पास इतना पानी है कि इन किसानों के खेत आराम से सींचे जा सकें। मगर प्रदेश में कैनाल बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया है।
“सरदार सरोवर का उदाहरण लें तो जब कोर्ट में इसकी ऊंचाई को लेकर केस चल रहा था तब गुजरात ने अपना कैनाल सिस्टम विकसित कर लिया। इसलिए केस ख़त्म होते ही वह बड़े हिस्से तक पानी पहुंचा रहा है. जबकि हमने ऐसी कोई तैयारी नहीं की।”
रामलाल नरते के परिवार की वार्षिक आमदनी 2 लाख रूपए है। मगर उनके 18 सदस्यों के संयुक्त परिवार के लिए यह काफी नहीं है। वह कहते है कि अगर उनके खेत तक पानी पहुंच जाएगा तो उनके बेटों को पलायन नहीं करना पड़ेगा और गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी।
मगर चाहे वह रामलाल नरते हों या फिर नारायण पटेल, किसानों तक पानी पहुंचाने के ज़रूरी है कि सरकार की प्राथमिकता सिंचाई की योजनाओं को अमल में लाना हो। अगर एक के बाद एक पावर प्रोजेक्ट लगते रहेंगे तो उनके घर का बल्ब तो जलेगा मगर चूल्हा नहीं।
भारत में स्वतंत्र पर्यावरण पत्रकारिता को जारी रखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट का आर्थिक सहयोग करें।
यह भी पढ़ें
वायु प्रदूषण से घुटते गांव मगर सरकारी एजेंडे से गायब
पातालकोट: भारिया जनजाति के पारंपरिक घरों की जगह ले रहे हैं जनमन आवास
किसान बांध रहे खेतों की मेढ़ ताकि क्षरण से बची रहे उपजाउ मिट्टी
खेती छोड़कर वृक्षारोपण के लिए सब कुछ लगा देने वाले 91 वर्षीय बद्धु लाल
पर्यावरण से जुड़ी खबरों के लिए आप ग्राउंड रिपोर्ट को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर अपने ईमेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जटिल शब्दावली सरल भाषा में समझने के लिए पढ़िए हमारी क्लाईमेट ग्लॉसरी।