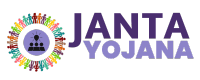Bihar 2005 Political Crisis (Photo: Social Media)
Bihar 2005 Political Crisis
साल 2005 का फरवरी महीना, बिहार की राजनीति में ऐसा तूफान लेकर आया जिसकी गूंज सिर्फ सत्ता के गलियारों में नहीं, बल्कि पूरे देश के राजनीतिक विमर्श में सुनाई दी। चुनाव के नतीजे आए, लेकिन सरकार नहीं बनी। नतीजों से ज़्यादा इस चुनाव को उसके बाद पैदा हुए संकट के लिए याद किया जाता है, जिसकी वजह बनी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान की एक असाधारण और अप्रत्याशित शर्त बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान होना चाहिए। इस एक मांग ने न सिर्फ सरकार गठन को रोका, बल्कि राज्य में अस्थिरता को जन्म दिया, जिसकी परिणति विधानसभा भंग होने और छह महीने के भीतर दोबारा चुनाव कराए जाने में हुई।
27 फरवरी 2005 को आए चुनावी नतीजों ने किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। आरजेडी, जो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन यह आंकड़ा बहुमत से काफी दूर था। कांग्रेस के 18 सीटों को मिलाकर यूपीए की कुल सीटें 93 ही थीं। वहीं एनडीए को 92 सीटें मिली थीं। लेकिन असली चौंकाने वाला आंकड़ा रहा रामविलास पासवान की लोजपा का, जिसने अकेले दम पर 29 सीटें जीतकर सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले ली।
यही वह मोड़ था जहां से बिहार की राजनीति ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। सभी को उम्मीद थी कि पासवान या तो यूपीए के साथ जाएंगे या एनडीए से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो शर्त रखी, उसने सभी राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया। पासवान ने खुद मुख्यमंत्री बनने की बजाय मांग की कि मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को बनाया जाए। यह राजनीतिक इतिहास में पहली बार था जब किसी दल ने सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी के लिए अपना दावा न ठोकते हुए किसी और को, वो भी किसी समुदाय विशेष से होने की शर्त पर समर्थन देने की बात कही।
रामविलास पासवान की इस मांग के पीछे उनकी रणनीति गहरी थी। वे गुजरात दंगों के बाद अल्पसंख्यकों के हितैषी के रूप में अपनी छवि गढ़ चुके थे और उन्हें लगता था कि मुसलमानों का नेतृत्व करने का नैतिक अधिकार अब उनके पास है। लालू यादव का एम-वाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण दशकों से बिहार की राजनीति पर हावी था। पासवान इस समीकरण को चुनौती देकर डीएम (दलित-मुस्लिम) समीकरण खड़ा करना चाहते थे, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वे राज्य की नई सामाजिक-राजनीतिक धुरी बन सकते हैं।
उन्होंने यहां तक प्रस्ताव दिया कि मुख्यमंत्री आरजेडी से ही हो, लेकिन कोई मुस्लिम नेता जैसे कि जाबिर हुसैन को बनाया जाए। लालू प्रसाद यादव इस शर्त से असहज थे। उन्हें डर था कि यदि सरकार की कमान किसी और के हाथ चली गई, तो पार्टी और सत्ता दोनों उनके हाथ से निकल जाएंगे, खासकर तब जब उन पर चारा घोटाले को लेकर दबाव लगातार बढ़ रहा था।
दूसरी ओर एनडीए, खासकर भाजपा, पासवान की इस मांग से साफ इनकार कर चुकी थी। भाजपा एक मुस्लिम मुख्यमंत्री के विचार से सहमत नहीं थी, और बिना भाजपा की सहमति के जदयू कोई भी सरकार नहीं बना सकता था। ऐसे में दोनों गठबंधनों ने रामविलास की शर्त को नकारते हुए सरकार गठन से हाथ पीछे खींच लिए।
राजनीतिक गतिरोध के बीच रामविलास पासवान के अपने विधायकों में भी असंतोष पनपने लगा। विधायकों ने चुनाव जीतने के लिए भारी संसाधन झोंके थे और वे सरकार में हिस्सेदारी चाहते थे। वे चाहते थे कि पासवान खुद मुख्यमंत्री बनने की मांग करें, लेकिन पासवान अपनी शर्त पर अडिग रहे। नतीजा ये हुआ कि लोजपा में टूट शुरू हो गई और उसके कई विधायक जदयू में शामिल हो गए। हालांकि संख्या इतनी नहीं थी कि सरकार बन सके, लेकिन इससे लोजपा की एकजुटता को गहरी चोट पहुंची।
स्थिति लगातार बिगड़ती देख राज्यपाल बूटा सिंह ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की और 7 मार्च 2005 को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। सरकार बनाने की कोई संभावना नजर न आने पर, अंततः 23 मई को विधानसभा को भंग कर दिया गया और नए चुनाव की घोषणा कर दी गई।
अक्टूबर 2005 में बिहार ने दोबारा मतदान किया, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। लोजपा, जिसने कुछ महीने पहले तक किंगमेकर की भूमिका निभाई थी, महज 10 सीटों पर सिमट गई। दूसरी ओर, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू और भाजपा गठबंधन ने बहुमत हासिल किया और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने।
रामविलास पासवान की शर्त ने उन्हें बिहार की सत्ता से दूर कर दिया, और उनकी राजनीतिक पकड़ कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंची जो उन्होंने 2005 में देखी थी। हालांकि वे केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे और कई सरकारों में मंत्री भी बने, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव सीमित होता चला गया। दूसरी ओर, नीतीश कुमार ने सत्ता की बागडोर संभालने के बाद बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल दी। वहीं लालू यादव और उनका परिवार अब तक सत्ता में वापसी नहीं कर पाया है।