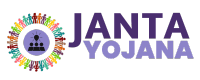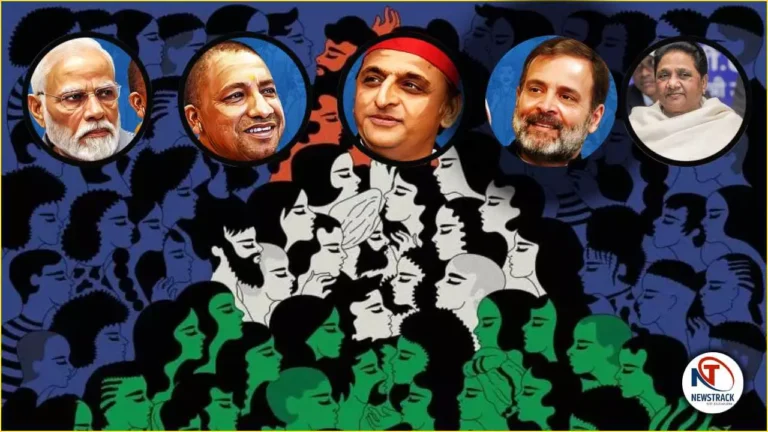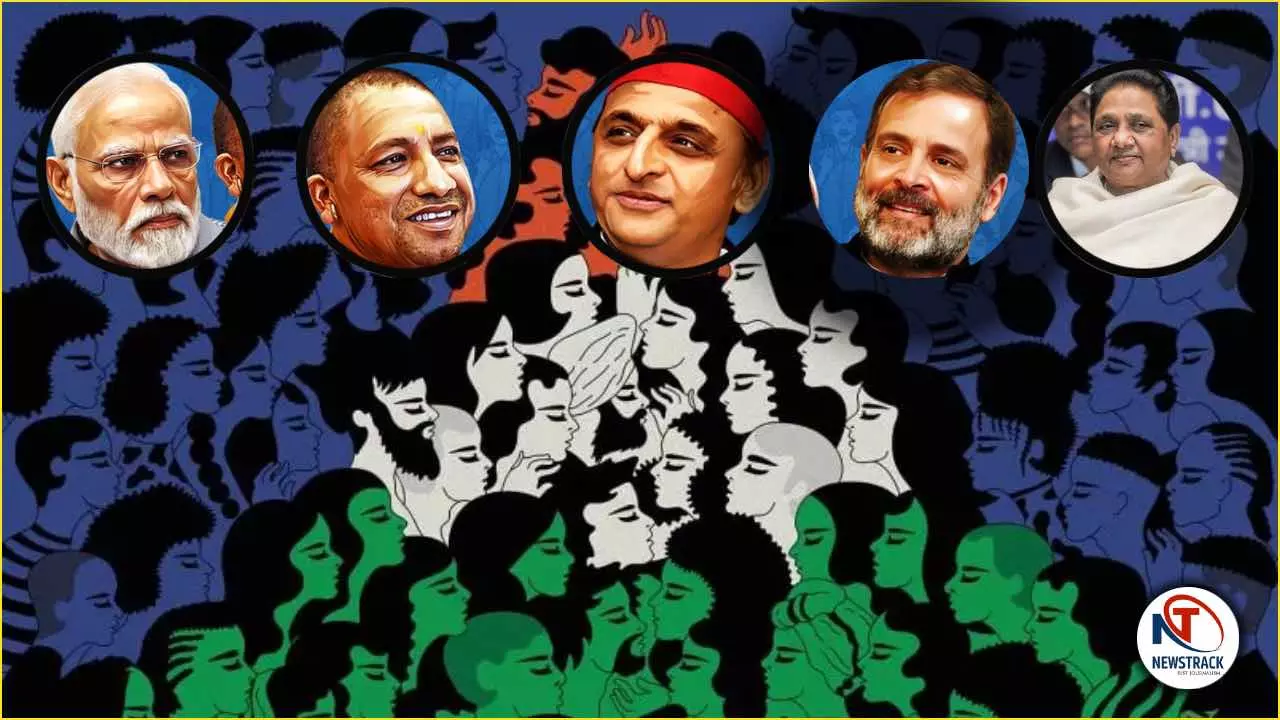
Caste Politics in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश, जिसे भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, वहां की चुनावी हवा जातीय समीकरणों से होकर ही बहती है। यह राज्य न केवल दिल्ली की सत्ता की चाबी संभालता है, बल्कि यहां की हर गली और गाँव में राजनीतिक चेतना जातीय पहचान से गहराई से जुड़ी होती है। कोई भी दल, चाहे वह सत्तारूढ़ हो या विपक्ष, तब तक निर्णायक नहीं हो सकता जब तक वह जातीय समीकरणों को समझ कर उनकी सही साधना न कर ले।
उत्तर प्रदेश की सामाजिक बनावट में ओबीसी सबसे बड़ा हिस्सा हैं — संख्या में लगभग आधे। इस वर्ग में यादव, कुर्मी, मौर्य, शाक्य, लोध, कश्यप, निषाद, राजभर जैसी अनेक जातियाँ हैं, जिनके राजनीतिक व्यवहार अलग-अलग हैं। यादवों की संख्या करीब छह प्रतिशत मानी जाती है, लेकिन संगठितता और नेतृत्व के कारण राज्य भर में इनका प्रभाव बहुत अधिक है। यही वर्ग समाजवादी पार्टी की रीढ़ रहा है, और अखिलेश यादव ने इसे केवल यादवों की पार्टी की छवि से निकालकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक — यानी PDA का नारा देकर व्यापक बनाने का प्रयास किया है।
यह नारा एक तरह से BJP की हिंदुत्व-आधारित राजनीति के समानांतर सामाजिक गठबंधन खड़ा करने की कोशिश है। अखिलेश चाहते हैं कि जिन जातियों को सत्ता से बाहर रखा गया, वे एक मंच पर आएं। दलितों के लिए BSP की गिरती पकड़ और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक बेचैनी इस प्रयोग को संबल देती है। लेकिन चुनौती यह है कि क्या यादवों के नेतृत्व में गैर-यादव OBC, जाटवों के बिना दलित और कांग्रेस के बिना अल्पसंख्यक लामबंद हो पाएंगे? PDA की राजनीति का प्रयोग 2024 के लोकसभा चुनावों में ज़मीन पर तो दिखा, लेकिन उसे निर्णायक सफलता में बदलने के लिए और समावेश की ज़रूरत है।
ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में करीब बारह प्रतिशत हैं। यह वर्ग परंपरागत रूप से भाजपा के साथ रहा है, लेकिन जब भी भाजपा ने इस वर्ग की उपेक्षा की है, तब उसके लिए असंतोष का स्वर मुखर हुआ है। 2007 में मायावती ने ब्राह्मण-दलित गठबंधन के ज़रिए सत्ता पाई थी, जो बताता है कि यह वर्ग सत्ता के समीकरण में अपने सम्मान की खोज करता है। ठाकुर यानी राजपूत समुदाय लगभग छह प्रतिशत हैं और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता के कारण भाजपा में इनकी हिस्सेदारी निर्णायक बन गई है। हालांकि यह भी सच है कि ठाकुर नेतृत्व के वर्चस्व से अन्य जातियों में असहजता की भावना बढ़ी है।
दलित — खासकर जाटव — बहुजन समाज पार्टी का आधार रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये वोट बिखरने लगे हैं। भाजपा ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के तहत गैर-जाटव दलितों को साधने में सफलता पाई है, वहीं समाजवादी पार्टी ने PDA के जरिए दलितों को नए रूप से जोड़ने की कोशिश की है। पर सच्चाई यह भी है कि जाटव मतदाता अब वैचारिक और सामाजिक अस्मिता की राजनीति के साथ-साथ अपने प्रतिनिधित्व को लेकर भी सतर्क हो गया है।
उत्तर प्रदेश के मुसलमान, जिनकी जनसंख्या लगभग उन्नीस प्रतिशत है, लंबे समय तक कांग्रेस और फिर समाजवादी पार्टी के साथ रहे। यह समुदाय अब ‘टैक्टिकल वोटिंग’ के रूप में राजनीतिक व्यवहार करता है। यानी जो पार्टी भाजपा को पराजित करने की स्थिति में दिखती है, मुसलमानों का बहुमत उसी ओर झुक जाता है। यही कारण है कि ओवैसी जैसी मुस्लिम पार्टियों का प्रवेश समाजवादी रणनीति को असहज करता है, और कांग्रेस से अल्पसंख्यक दूरी भी S.P. के लिए अवसर बनती है।
पूर्वांचल में निषाद, राजभर, मल्लाह, कुशवाहा, पटेल जैसी जातियाँ निर्णायक हैं। यह जातियाँ परंपरागत रूप से OBC में आती हैं लेकिन यादवों के वर्चस्व के खिलाफ लामबंद रही हैं। भाजपा ने इसी खाई को समझा और निषाद पार्टी व सुभासपा जैसे सहयोगी बनाकर इन्हें अपने साथ जोड़ा। इस क्षेत्र में भाजपा की सफलता की एक बड़ी वजह यह भी है कि उसने इन जातियों को सत्ता और संगठन में हिस्सेदारी दी। यही फॉर्मूला भाजपा अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों और अन्य OBC वर्गों के साथ भी अपनाने की कोशिश कर रही है।
शहरी सीटों पर कायस्थ, बनिया, पंजाबी, भूमिहार जैसी जातियाँ निर्णायक होती हैं। यह वर्ग आर्थिक मुद्दों, कानून व्यवस्था और विकास के सवालों को लेकर मतदान करता है और भाजपा के शहरी एजेंडे का प्रमुख समर्थक बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों की उपस्थिति भी कुछ सीटों पर समीकरण बदल सकती है, खासकर तब जब मुद्दा आर्थिक असमानता या स्थानीय भ्रष्टाचार बनता है।
उत्तर प्रदेश में जातियों की केवल गणना नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक चेतना, संगठन, नेतृत्व और समर्पण तय करता है कि कौन किस ओर जाएगा। यही कारण है कि PDA जैसा सामाजिक गठबंधन हो या हिंदुत्व आधारित समावेशन — दोनों को जमीन पर उतारने के लिए केवल नारा नहीं, बल्कि ठोस कार्यक्रम, प्रतिनिधित्व और संवाद की ज़रूरत है।
2027 के चुनाव अब केवल जाति जोड़ने का गणित नहीं रहेंगे, बल्कि यह देखना होगा कि कौन जाति के पार जाकर संवाद बना सकता है, नेतृत्व दे सकता है और विश्वास अर्जित कर सकता है। जब तक राजनीति केवल पहचान आधारित रहेगी, तब तक सत्ता पाने के लिए जातीय संतुलन साधना अनिवार्य रहेगा। लेकिन भविष्य की राजनीति उस मोड़ पर आ खड़ी है जहाँ प्रतिनिधित्व के साथ-साथ समावेशन और संवाद, सत्ता की असली कुंजी होंगे।