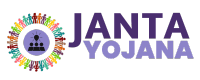मध्य प्रदेश के मंडला ज़िला मुख्यालय से 62 किमी दूर चुटका गांव में पंचायत जमी हुई है। चुटका, टाटीघाट और कुंडा सहित कई गांव के लोगों का जुटान हुआ है। लोगों में असुरक्षा का भाव है। वह अपने संभावित विस्थापन पर चिंता जता रहे हैं और उससे बचने के लिए सलाह कर रहे हैं।
दरअसल बीते दिसंबर मध्य प्रदेश के चार ज़िलों में न्यूक्लियर पॉवर प्लांट्स स्थापित करने की मंजूरी मिली है। इसमें चुटका से महज़ कुछ किमी दूर स्थित सिवनी का किंदरई पॉवर प्लांट भी शामिल है। इस घोषणा के बाद सिवनी जिले में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जबकि चुटका में विस्थापन को लेकर आशंकाएं और बढ़ गई हैं।
दरअसल 2009 में न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने चुटका में पॉवर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया था। हालांकि 1400 मेगावाट (2×700 मेगावाट) के इस प्लांट को 15 जून 2017 में वित्तीय मंजूरी मिली थी। इससे लगभग 54 गांव प्रभावित होने का अनुमान है। इनमें से चुटका को पूरी तरह से वहीं कुंडा और टाटीघाट को आंशिक रूप से विस्थापित किया जाना है।
प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद भी स्थानीय लोगों के विरोध के चलते अब तक विस्थापन नहीं हुआ है। मगर किंदरई में पॉवर प्लांट लगने की संभावनाओं ने चुटका के निवासियों को डर में डाल दिया है। इसे ऐसे समझिए कि गांव के एक बुजुर्ग से इस बारे में बात करने पर वह निराशा से बस इतना कहते हैं,
“सबसे पहले चुटका ही उठेगा (विस्थापित होगा), हम कहां जाएंगे?”
मध्य प्रदेश के 4 जिलों में लगने हैं पॉवर प्लांट
मध्य प्रदेश के सिवनी के अलावा देवास, नीमच और शिवपुरी में 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। यह प्लांट 1200 मेगावाट के होंगे जहां 2 से 6 यूनिट स्थापित की जाएंगी। इसके लिए 1200 से 2000 एकड़ तक भूमि की आवश्यकता होगी।
किंदरई में पॉवर प्लांट के विरोध में बनी क्षेत्रीय जन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष डीपी गिरयाम बताते हैं कि स्थानीय अखबार में पॉवर प्लांट की खबर पढ़ने के बाद ग्रामीणों में असुरक्षा का माहौल बना है। गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग बरगी बांध परियोजना से पहले से ही विस्थापित हैं।
स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी ज़्यादा है कि ग्रामसभा को इस बारे में अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है। जबकि पेसा (PESA) कानून के तहत ऐसा किया जाना अनिवार्य है। गिरयाम कहते हैं,
“सरकार हमको विस्थापित करने वाली है मगर हमें ही कुछ नहीं बता रही है.”
हाल ही में यहां कुछ सरकारी अधिकारी सर्वे करने पहुंचे थे। मगर इसका स्थानीय ग्रामीणों ने बहुत विरोध किया। उनका कहना है कि प्रशासनिक अमला बिना किसानों की अनुमति के उनके खेतों का सर्वे कर रहा था। इस कार्यवाही से स्थानीय लोगों सहित आस-पास के गांव में विस्थापन का डर बैठ गया है। इसके चलते चुटका में भी ग्रामसभा आयोजित की जा रही है।
चुटका में आशंकाएं क्यों बढ़ गई हैं?
चुटका में न्यूक्लियर पॉवर प्लांट बनाने का निश्चय 2009 में किया गया था। मगर 2025 में भी ‘ग्रीन फील्ड’ उजाड़ और बंजर पड़ा हुआ है। स्थानीय विरोध के चलते यहां अब तक निर्माण शुरू नहीं हो सका है।
मई 2023 में नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (NTPC) लिमिटेड ने न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है। इस समझौते के अनुसार अब दोनों कम्पनियां मिलकर चुटका एटॉमिक पॉवर प्रोजेक्ट और माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पॉवर प्रोजेक्ट (4×700 MV) का निर्माण करेंगी।
दिसंबर 2023 में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि चुटका पॉवर प्लांट के लिए कुल 708.19 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। 21,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट से विस्थापित होने वाले लोगों को मुआवज़ा और उनके लिए कॉलोनी का निर्माण भी किया जा चुका है।
यह भी बताया गया कि प्रभावित गांव अब तक खाली नहीं करवाए गए हैं। साथ ही इस परियोजना को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।
यानि बीते एक-डेढ़ साल में परियोजना को लेकर जो-जो डेवलपमेंट हुए हैं, उसने ग्रामीणों को फिर से विस्थापित हो जाने के डर से मुक्त नहीं होने दिया था। अब किंदरई में पॉवर प्लांट की स्थापना को लेकर की जा रही कार्यवाही इसे और पुख्ता कर रही है।
“आज़ादी के बाद से ही विस्थापन की बिमारी लगी हुई है”
जनवरी के जाड़े की रात में मैं चुटका गांव में भगवती बाई के कच्चे मकान में आलाव के पास बैठा हुआ हूं। दिन में गांव में एक बोर्ड दिखा था जिस पर लिखा था कि यह गांव ‘खुले में शौच मुक्त’ यानि ओडीएफ प्लस गांव है। मगर पूरे गांव में कहीं भी शौचालय नहीं दिखाई देता।
इसका कारण मैं भगवती बाई (56) से पूछता हूं तो वो कहती हैं,
“विकास हो ही नहीं पाता हमारा, आज़ादी के बाद से ही विस्थापन की बिमारी लगी रही।”
दरअसल चुटका परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी लोग बरगी बांध से विस्थापित हैं। ऐसे में यह उनका दोबारा विस्थापन होगा। टाटीघाट के रहने वाले 58 वर्षीय श्यामलाल बर्मन भी इनमें शामिल हैं।
बर्मन बताते हैं कि उनके पिता काश्तकार (किसान) हुआ करते थे। उनके पास 11 एकड़ कृषि भूमि और 2 कछार हुआ करते थे। मगर बरगी परियोजना में उनकी पूरी ज़मीन डूब गई। अब वो भूमिहीन हैं। उन्होंने बताया कि बरगी में डूबी ज़मीन के लिए यहां के लोगों को 600 रु से 1500 प्रति एकड़ की दर से मुआवज़ा दिया गया था।
श्यामलाल बर्मन के परिवार में कुल 7 लोग हैं। मगर कृषि के आभाव में परिवार का पालन करना बेहद मुश्किल हो गया है।
जैसा की नाम से स्पष्ट है, टाटीघाट नर्मदा नदी के ठीक बगल में स्थित है। यहां लगभग 42 मछुआरों का परिवार रहता है। मगर यह सब शिकायत करते हैं कि नदी में मछली कम हैं ऐसे में इनको बेचकर परिवार चलाना मुश्किल है।
“20 रूपए किलो मछली का रेट है, इसमें 5 रू महासंघ को देने होते हैं। यानि एक किलो मछली बेचकर हम 15 रू ही कमा पा रहे हैं।”
बर्मन बताते हैं कि वह दिन भर में 2 किलो मछली ही पकड़ पाते हैं। इससे होने वाली कमाई से परिवार की ज़रूरतों को पूरी करना मुश्किल है। इसलिए उनके दोनों बेटे पलायन करके मज़दूरी करने जाते हैं। बर्मन कहते हैं कि गांव के सभी घरों का यही हाल है। यहां जनवरी के महीने में 42 में से 22 परिवार ही गांव में हैं बाकी सब पलायन पर हैं।
अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि को बताते हुए वह कहते हैं कि उनके पास जमा पूंजी नहीं है। यह रोज़ कमाने और खाने का संघर्ष है। ऐसे में विस्थापित होकर बाहर जाना और वहां अपना घर बसाना मुमकिन नहीं है।
दरअसल साल 2015 में 450 परिवारों को कुल 41.6 करोड़ रूपए का मुआवज़ा दिया गया था। मगर चुटका, कुंडा और टाटीघाट तीनों ही गांव के लोगों का कहना है कि उनके खाते में मुआवजा की राशि बिना उनकी जानकारी के डाली गई थी।
बर्मन अभी 2,352 वर्ग फीट के कच्चे मकान में रहते हैं। इस मकान के लिए उन्हें मुआवज़े के रूप में 2.58 लाख रूपए मिले हैं। इसके अलावा उन्हें 6 लाख 25 हजार रु का मुआवजा पैकेज मिला है। मगर वह कहते हैं कि विस्थापन से होने वाली हानि इस राशि से ज़्यादा बड़ी है।
“हम पहले किसान थे, फिर ज़मीन गई तो मछलीपालन पे गुजारा किया अब इसको छोड़कर नया काम कहां से सीखेंगे?”
दरअसल टाटीघाट के मछुआरों का तर्क है कि जहां उन्हें पुनर्वास करके बसाया जा रहा है वहां उनके लिए आजीविका का कोई साधन नहीं है।
दरअसल इस क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास के लिए मंडला जिले के ही गोंझी ग्राम में कॉलोनी का निर्माण किया गया है। मगर ज़िला मुख्यालय से लगभग 50 किमी दूर स्थित इस गांव के आस-पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है।
“मंडला में न तो कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ना ही कोई बड़ा जलाशय है कि मछली पकड़ी जा सके।”
किसान से मज़दूर बन जाने का ख़तरा
चुटका गांव के दादुलाल (64) लगभग 10 एकड़ में खेती करते हैं। वह हमें अपनी गेहूं और मटर की फसल दिखाते हुए कहते हैं कि ये ‘सोने की ज़मीन’ है। वह बताते हैं कि उन्होंने आज तक बिना किसी रसायन का प्रयोग किए ही खेती की है। उनके अनुसार भले ही सरकार इसे ‘बर्रा ज़मीन’ (पथरीली ज़मीन) कह रही हो मगर इसमें उन्हें भरपूर उत्पादन मिलता है।
वह समझाते हुए कहते हैं कि अभी फसलों में रासायनिक ऊर्वरकों का इस्तेमाल न होने से वह कम लागत में खेती कर लेते हैं। मगर विस्थापन के बाद वह भूमिहीन हो जाएंगे जिससे उन्हें आजीविका के लिए मज़दूरी पर निर्भर होना पड़ेगा। वह भी श्यामलाल बर्मन की बातें ही दोहराते हुए कहते हैं कि केवल मज़दूरी से आजीविका चलाना मुश्किल है।
दादुलाल के लिए यह विस्थापन केवल उनका पता बदलने तक सीमित नहीं है। वह कहते हैं,
“हम लोग आदिवासी काश्तकार हैं। जंगल के बीच रहते हैं। यहां हम ज़मीन के मालिक हैं वहां जाकर हम मज़दूर बनकर रह जाएंगे।”
दादुलाल के पास 4 गाय और लगभग इतनी ही भैंस हैं। मगर उन्हें इनका कोई भी मुआवज़ा नहीं मिला। वह कहते हैं कि गोंझी में स्थित पुनर्वास कॉलोनियों में इन जानवरों को बांधने की जगह नहीं है। मज़दूरी करके परिवार का पेट पालना ही मुश्किल होगा तो जानवरों को वो क्या खिलाएंगे?
दादुलाल कहते हैं कि अभी उनके खेत से निकलने वाला चारा और जंगल में उगने वाली घास से उनके जानवरों को भोजन मिल जाता है मगर जंगल से दूर जाते ही यह भी मुश्किल हो जाएगा।
रेडिएशन और पानी से संबंधित असुरक्षाएं
गोंड आदिवासी समुदाय से आने वाले रामलाल नरते (68) कुंडा गांव में रहते हैं। वह 20 एकड़ में खेती करते हैं। कुंडा गांव चुटका परियोजना से आंशिक रूप से ही विस्थापित होने वाला है। नरते विस्थापित होने वाले लोगों में शामिल नहीं हैं। मगर फिर भी वह इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।
नरते सहित कुंडा, चुटका और टाटिघाट के कई लोगों ने राजस्थान के रावतभाटा न्यूक्लियर पॉवर प्लांट का दौरा किया था। उन्हें रावतभाटा के लोगों ने न्यूक्लियर पॉवर प्लांट से होने वाले रेडिएशन के बारे में बताया था। गौरतलब है कि जुलाई 2012 में रावतभाटा के प्लांट में ट्राईटियम रेडिएशन की खबर को कई राष्ट्रिय दैनिकों ने कवर किया था। 2012 में इस पॉवर प्लांट में महज़ के महीने के अंतराल में ही 6 लोग रेडिएशन से सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे।
अब कुंडा और अन्य गांव के लोगों को डर है कि अगर पॉवर प्लांट बनता है तो उसके रेडिएशन से वो भी प्रभावित होंगे। चुटका परियोजना के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट कर आंदोलन खड़ा करने वाले राजकुमार सिंहा (60) भी रेडिएशन के सवाल को उठाते हुए कहते हैं
“यह कहा जाता है कि यह (न्यूक्लियर पॉवर प्लांट) एक क्लीन एनर्जी है मगर असल में ये क्लीन है नहीं।”
न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम डाईऑक्साइड (UO2) और हैवी वाटर (Deuterium Oxide) का इस्तेमाल किया जाता है। ईधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम डाईऑक्साइड रेडियोएक्टिव पदार्थ है। नीरी (NEERI) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार इस प्लांट से तरल और गैस अवस्था में रेडियोन्यूक्लाइड्स (Radionuclides) होंगे।
रिपोर्ट के अनुसार (पेज 6) प्लांट के बाहर रहने वाले लोग हर साल 0.11 mSv रेडिएशन अवशोषित (dose limit) कर रहे होंगे। जबकि चुटका न्यूक्लियर पॉवर प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ऐसे व्यवस्था बनाई जाएगी कि 5 साल में उन्हें कुल 100 mSv रेडिएशन ही अवशोषित करना पड़े।
एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (AERB) के मानकों के अनुसार आम जनता के लिए यह लिमिट 1 mSv प्रति साल है। जबकि कर्मचारियों के लिए यह 20 mSv प्रति साल है। यानि सरकारी कागज़ों में यह प्लांट रेडिएशन के सरकारी मानकों का पालन करते हुए नज़र आता है।
मगर राजकुमार सिंहा नीरी की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करते हैं। वह कहते हैं कि यह संस्था सभी परियोजनाओं की पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट सरकार की मंशा के अनुकूल बनाती है, इस परियोजना के प्रभावों का भी उसने बहुत सतही अध्ययन किया है।
साउथ एशियन पीपल्स एक्शन ऑन क्लाइमेट क्राइसिस (SAPACC) के को-कन्वीनर डॉ सौम्या दत्ता भी प्लांट के रेडिएशन पर चिंता व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं,
“यूरेनियम (U235) के दहन (fission) से आयोडीन (I-131) सहित कई रेडियो एक्टिव गैस निकलती हैं। यह वायुमंडल के ज़रिए मानव शरीर में पहुंचती हैं।”
वह कहते हैं कि इससे बच्चे और गर्भवती महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं। साथ ही इससे आस-पास रहने वाले लोगों की आने वाली पीढ़ी के डीएनए में भी बदलाव आएंगे।
राजकुमार सिंहा कहते हैं कि रेडिएशन के साथ-साथ इस पॉवर प्लांट द्वारा नर्मदा नदी की इकोलॉजी भी प्रभावित होगी। दरअसल इस प्लांट को हर घंटे 9000 क्यूबिक मीटर पानी की ज़रूरत होगी। इस पानी की आपूर्ति नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध से ही की जाएगी।
जलाशय से लिए जाने वाले कुल पानी में से 2660 क्यूबिक मीटर पानी वापस बांध में ही वापस छोड़ दिया जाएगा। मगर इसे लेकर डॉ दत्ता चिंता ज़ाहिर करते हैं। वह कहते हैं कि मछलियां पानी के तापमान को लेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं। ऐसे में अगर रिएक्टर से निकलने वाले गर्म पानी को वापस जलाशय में छोड़ा जाएगा तो उससे मछलियां और नदी की इकोलॉजी पर असर पड़ेगा।
साल 2009 से लेकर अब तक दादुलाल सहित चुटका और अन्य प्रभावित गांवों के लोग एक अनिश्चितता में जी रहे हैं। इसके चलते यहां का विकास भी पूरी तरह रुक गया है। दादुलाल चाहते हैं कि वह अपने घर में शौचालय का निर्माण करवा लें मगर यह घर कब खाली करना पड़ जाए यह कोई नहीं जानता। मगर दादुलाल कहते हैं कि वह इस जगह से नहीं हटेंगे ‘अगर सरकार चाहे तो हमको मार भी दे मगर हम नहीं हटेंगे।’
भारत में स्वतंत्र पर्यावरण पत्रकारिता को जारी रखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट का आर्थिक सहयोग करें।
यह भी पढ़ें
वायु प्रदूषण से घुटते गांव मगर सरकारी एजेंडे से गायब
कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र ‘हरित समाधान’ या गाढ़ी कमाई का ज़रिया?
पातालकोट: भारिया जनजाति के पारंपरिक घरों की जगह ले रहे हैं जनमन आवास
खेती छोड़कर वृक्षारोपण के लिए सब कुछ लगा देने वाले 91 वर्षीय बद्धु लाल
पर्यावरण से जुड़ी खबरों के लिए आप ग्राउंड रिपोर्ट को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर अपने ईमेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जटिल शब्दावली सरल भाषा में समझने के लिए पढ़िए हमारी क्लाईमेट ग्लॉसरी।